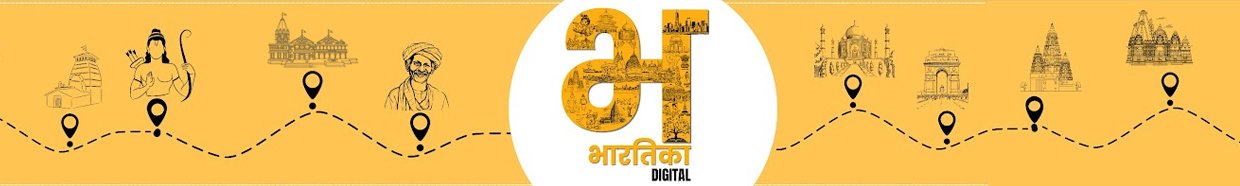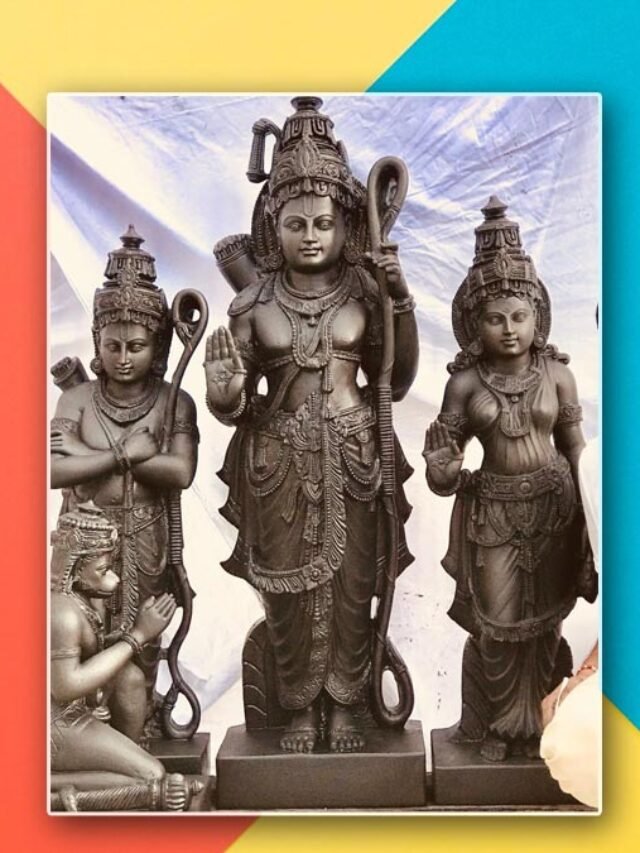नेपाल एक बार फिर संकट में है। यह संकट सिर्फ़ राजनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है। सवाल यह है कि बार-बार अस्थिरता की पटकथा कौन लिख रहा है? जनता के भरोसे को तोड़ने वाली यह राजनीति आख़िर किसके हित में है?
सत्रह साल में पंद्रह सरकारें बदलना किसी लोकतंत्र का सामान्य क्रम नहीं हो सकता। यह अस्थिरता बताती है कि नेपाल की राजनीति जनता की आकांक्षाओं के बजाय सत्ता समीकरणों और बाहरी दबावों की कैद में है। जनता हर चुनाव के साथ स्थिरता चाहती है, लेकिन नतीजा वही—गठबंधन की गुत्थी, कुर्सी की खरीद-फ़रोख़्त और नेताओं की अदूरदर्शिता। यही वजह है कि आज काठमांडू की गलियों और गाँवों में राजशाही की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। लोग पूछ रहे हैं—क्या लोकतंत्र हमें स्थिरता नहीं दे सकता?
पर असली सवाल यह भी है कि यह अस्थिरता कहीं दूर से तो नहीं संचालित हो रही? नेपाल की राजनीति में अमेरिकी डीप स्टेट की छाया साफ तौर पर बार-बार दिखाई देती है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर अमेरिकी संस्थान और उनसे जुड़े नेटवर्क नेपाल ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सत्ता परिवर्तन के सूत्रधार बने हुए हैं।
यह ढाँचा नया नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का पतन, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के ख़िलाफ़ अचानक उभरे जनआंदोलन, बांग्लादेश में उत्पात और अमेरिकी पिट्ठू यूनुस की सत्तापोशी, मालदीव में चीन-भारत की खींचतान के बीच अचानक हुए सत्ता परिवर्तन और अफगानिस्तान में दशकों तक अस्थिरता का माहौल। हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। जनता की हताशा को हवा दी जाती है, आंदोलन संगठित होते हैं, मीडिया और एनजीओ सक्रिय हो जाते हैं, और सत्ता की बागडोर बदल जाती है। यह सब संयोग नहीं है, यह रणनीति है—अमेरिकी डीप स्टेट की। नेपाल इसका अपवाद नहीं है।
नेपाल की अर्थव्यवस्था इस राजनीति का सबसे बड़ा शिकार बनी है। मुश्किल से 45 अरब डॉलर की जीडीपी, जिसमें 25-30 प्रतिशत हिस्सा रेमिटेंस का है। पर्यटन, जिस पर देश की पहचान टिकी है, लगातार गिरावट में है। बेरोज़गारी 11-12 प्रतिशत के आसपास और युवा पलायन जारी। महंगाई ने आम परिवार की कमर तोड़ दी है। राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेश रोक दिया है। मौजूदा संकट ने देश की जीडीपी को और कमज़ोर किया है—बिहार जैसे एक भारतीय राज्य की अर्थव्यवस्था भी नेपाल से कहीं आगे निकल चुकी है। इस पूरी स्थिति में जनता, सबसे बड़ी हारी हुई ताक़त है। लोकतंत्र से जो उम्मीदें थीं, वे टूट रही हैं। जनता अब विकल्प तलाश रही है—और यही जगह है जहाँ डीप स्टेट और बाहरी ताक़तें सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। निराश जनता को या तो राजशाही की याद दिलाई जाती है या फिर किसी नए नेता के चेहरे पर उम्मीद का रंग पोता जाता है।
असल संकट यही है कि नेपाल अब केवल अपनी राजनीति से नहीं चल रहा, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के रणनीतिक खेल का मोहरा बन चुका है। हिमालय के इस छोटे देश में सत्ता का हर परिवर्तन एशिया की बड़ी तस्वीर को प्रभावित करता है और यही वजह है कि अमेरिकी डीप स्टेट यहाँ लगातार सक्रिय है। कभी आर्थिक दबाव, कभी एनजीओ नेटवर्क, कभी लोकतंत्र के नाम पर विदेशी सहायता। आज नेपाल जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ से दो रास्ते हैं, या तो वह जनता की उम्मीदों को केंद्र में रखकर स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए, या फिर बाहरी ताक़तों और डीप स्टेट की योजनाओं का खिलौना बना रहे।
जनता का सवाल साफ़ है—हम स्थिरता चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, भविष्य चाहते हैं। लेकिन सत्ताधारी वर्ग और बाहरी ताक़तें इन सवालों को सुनना ही नहीं चाहतीं। यही कारण है कि नेपाल का संकट केवल उसका अपना संकट नहीं है, यह दक्षिण एशिया के जियो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। अंततः सवाल यही है—क्या नेपाल अपनी किस्मत खुद लिखेगा या फिर यह पटकथा हमेशा बाहर लिखी जाएगी?
लोकतंत्र से मोहभंग, आर्थिक अनिश्चितता और डीप स्टेट की परछाईं—ये तीनों मिलकर जनता के भीतर राजशाही की वापसी की चाह को हवा दे रहे हैं। यह चाह शायद नॉस्टैल्जिया हो, लेकिन यह भी सच है कि लोकतंत्र की नाकामियां ही इसे जन्म देती हैं।नेपाल का संकट किसी एक बाहरी ताक़त का खेल नहीं है। यह असल में भीतर की कमजोरी और परदे के पीछे सक्रिय डीप स्टेट का परिणाम है। जब तक नेपाल की राजनीति जनता के सवालों को केंद्र में नहीं लाएगी और संस्थान पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक काठमांडू की सत्ता बार-बार बदलती रहेगी और जनता बार-बार वही सवाल पूछेगी—नेपाल का मालिक कौन है?
– अनुरंजन झा
(लेखक, गांधियन पीस सोसायटी, ब्रिटेन के चेयरपर्सन और भारतिका मीडिया के संस्थापक हैं)