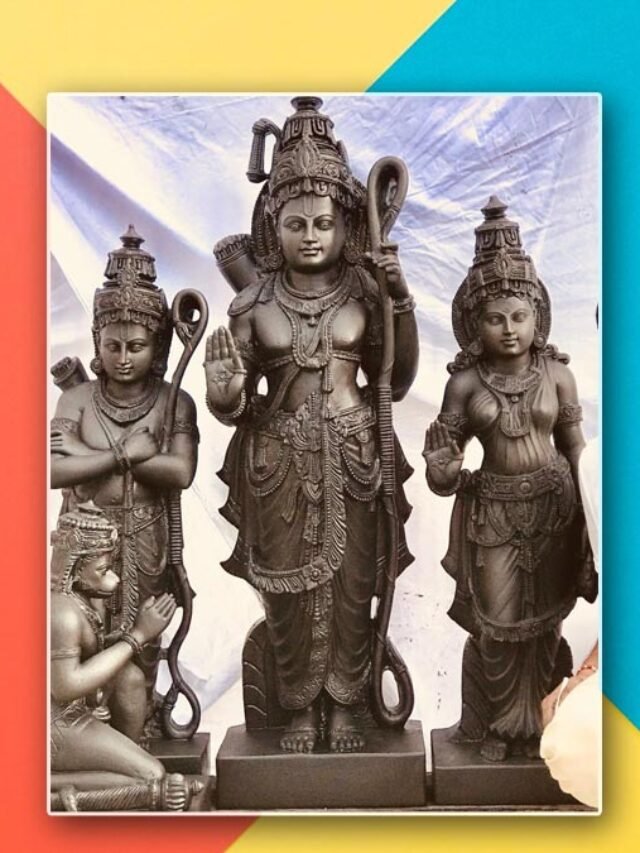भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पहले ही अनेक दबावों से जूझ रही है। गिरती गुणवत्ता, बेरोज़गारी से जूझते ग्रेजुएट्स, संसाधनों की कमी और बेतहाशा कंपटीशन। ऐसे समय में यदि नियामक संस्थाएँ ऐसे नियम लेकर आएँ, जो समाधान से ज़्यादा नई आशंकाएँ पैदा करें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। UGC के हालिया नियमों को लेकर उपजा विवाद केवल एक प्रशासनिक बहस नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक ताने-बाने से जुड़ा है, जिसे संभालने की ज़िम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था पर भी होती है।
नए नियमों का घोषित उद्देश्य जातिगत भेदभाव को रोकना और कैंपस को “समान” व “सुरक्षित” बनाना है। उद्देश्य सुनने में नेक है। कोई भी सभ्य समाज भेदभाव का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन समस्या नीयत में नहीं, संरचना में है। जब नियम इस तरह गढ़े जाएँ कि वे एक पूरे वर्ग को संभावित पीड़ित और दूसरे को संभावित अपराधी की तरह देखने लगें, तो वे न्याय नहीं, बल्कि अविश्वास पैदा करते हैं।
इन नियमों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि शिकायत की संरचना एकतरफ़ा दिखाई देती है। SC/ST/OBC की शिकायत को संस्थागत रूप से प्राथमिकता मिलेगी यह अपने-आप में गलत नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक अन्याय को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका व्यावहारिक नतीजा क्या होगा? शिकायत सुनी जाएगी, जाँच बैठेगी, माहौल बनेगा और जिसके खिलाफ शिकायत होगी, वह लगभग तय रूप से “सामान्य वर्ग” से होगा। यानी एक पूरे वर्ग को पहले ही नैरेटिव में संदिग्ध बना दिया गया। यहाँ सवाल यह नहीं है कि भेदभाव होता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हर शिकायत अपने-आप में सत्य मानी जाएगी? क्या जाँच की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय “पहले सुनो, फिर तय करो” का संतुलन बना रहेगा? नियमों की भाषा और समय-सीमा यह आभास देती है कि आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा, न कि शिकायतकर्ता को आरोप सिद्ध करना। यह न्याय का सिद्धांत नहीं, उलटा बोझ (reverse burden) है।
शिक्षा का परिसर अदालत नहीं होता, और न ही पुलिस थाना। वहाँ विचारों का टकराव होता है, मतभेद होते हैं, बहस होती है और कई बार तीखी भी। यदि हर असहमति, हर अनुशासनात्मक कार्रवाई, हर अकादमिक निर्णय को “जातिगत विद्वेष” के चश्मे से देखा जाने लगेगा, तो सबसे पहले अकादमिक स्वतंत्रता कुचली जाएगी। शिक्षक डरे रहेंगे, प्रशासन असमंजस में रहेगा, और छात्र समूहों में बँटते चले जाएँगे। एक और गंभीर चिंता दुरुपयोग की है। हमारे सामाजिक यथार्थ में यह मान लेना भोलेपन से कम नहीं कि हर कानून या नियम का दुरुपयोग नहीं होगा। जब शिकायतकर्ता के लिए कोई जवाबदेही तय न हो, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर स्पष्ट दंड न हो, तो डर पैदा होता है। करियर, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य तीनों एक शिकायत से प्रभावित हो सकते हैं। क्या व्यवस्था इसके लिए तैयार है?
यह भी समझना होगा कि आज का सामान्य वर्ग का छात्र किसी “सत्ता” की सहज स्थिति में नहीं है। निजी शिक्षा महँगी है, सरकारी अवसर सीमित हैं, प्रतियोगिता तीखी है। वह पहले ही खुद को हाशिये पर महसूस करता है। ऐसे में यदि नियम उसे यह संकेत दें कि वह “संभावित अपराधी” है, तो यह भावना और गहरी होगी और यही भावना आगे चलकर सामाजिक कटुता का रूप लेती है। विडंबना यह है कि समानता के नाम पर बनाए गए नियम अगर समाज को और खाँचों में बाँट दें, तो वे अपने ही उद्देश्य को विफल कर देते हैं। वास्तविक समानता का मतलब है कि नियम सबके लिए एक जैसे हों, जाँच निष्पक्ष हो, और जब तक दोष साबित न हो जाए, किसी को अपराधी न माना जाए। अगर किसी व्यवस्था में एक पक्ष की बात पहले ही सच मान ली जाए और दूसरे पक्ष को पहले से शक के घेरे में डाल दिया जाए, तो उसे समानता नहीं कह सकते। वह न्याय नहीं, बल्कि चुनिंदा न्याय है जो दरअसल भेदभाव है।
सत्ताधारी कुछ नेता “मोदी है तो मुमकिन है” जैसे नारों के सहारे यह साबित करने में लगे हैं कि नए नियमों से कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भरोसा ज़्यादा राजनीतिक मजबूरी से पैदा हुआ लगता है, नैतिक स्पष्टता से नहीं। सत्ता में बने रहने की जुगत में अगर सवर्ण समाज की आशंकाएँ अनदेखी की जा रही हैं, तो यह भी एक तरह की राजनीति ही है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है सवर्ण पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं की चुप्पी। इस मुद्दे पर उनका मौन किसी संतुलन का नहीं, बल्कि वोट-बैंक गणित का नतीजा दिखाई देता है। कागज़ों पर लिखे नियम साफ़ संकेत देते हैं कि व्यवस्था पहले ही दिन से एक वर्ग को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है।
जब नियम ही यह मानकर बनाए जाएँ कि कौन शिकायत करेगा और किसके खिलाफ होगी, तो यह निष्पक्षता नहीं रहती। ऐसे में यह कहना कठिन हो जाता है कि यह केवल भेदभाव रोकने की कोशिश है—क्योंकि व्यवहार में यह नए सिरे से भेदभाव की ज़मीन तैयार करती दिखती है। भारत जैसे विविध समाज में शिक्षा ही वह जगह है, जहाँ संवाद, सहअस्तित्व और आपसी सम्मान की संस्कृति विकसित होनी चाहिए। यदि कैंपस डर, शिकायत और शक के माहौल में बदलेंगे, तो वहाँ से न ज्ञान निकलेगा, न नेतृत्व। ज़रूरत ऐसे नियमों की है, जो भेदभाव को रोकें, लेकिन बिना नए भेदभाव को जन्म दिए। जो पीड़ित को सुरक्षा दें लेकिन निर्दोष को भयभीत न करें।
UGC को चाहिए कि वह इन नियमों की समीक्षा करे, सभी वर्गों की आशंकाएँ सुने, और ऐसी संतुलित प्रक्रिया बनाए जिसमें शिकायत की जाँच निष्पक्ष हो, दुरुपयोग पर अंकुश हो, और किसी भी छात्र को उसकी जाति के आधार पर पहले से अपराधी या पीड़ित न माना जाए। वरना खतरा यही है कि हम जातिगत विद्वेष को कम करने के बजाय, उसे संस्थागत रूप दे बैठेंगे और शिक्षा, जो समाज को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, वही विभाजन का अखाड़ा बन जाएगी।
अनुरंजन झा
चेयरमैन, गांधियन पीस सोसायटी, ब्रिटेन