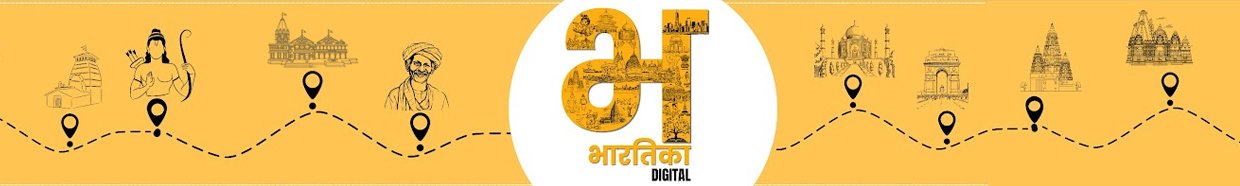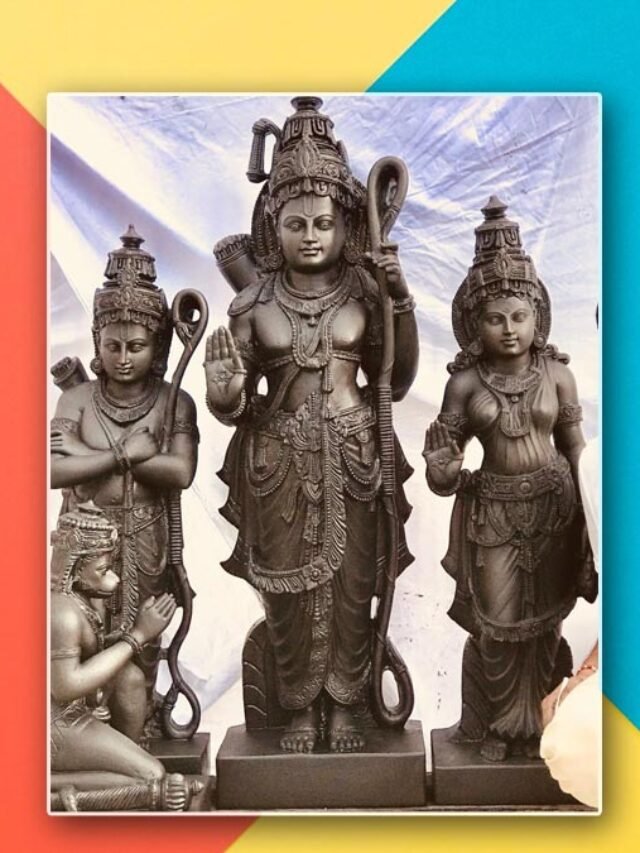स्वर्गीय पंडित छन्नू लालमिश्र जी से मेरा साक्षात्कार केवल एक बार ही हुआ था जब भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के महानिशेक के रूप में २०१९ में वाराणसी यात्रा के बीच पंडित जी के प्रति उनकी अप्रतिम भारतीय संगीत साधना और संस्कृति की आजीवन सेवा के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने गया था । बनारसी फक्कडपन की अनौपचारिता के आकर, मैं अपनी अर्धांगिनी रीति के साथ, अपने बाल्यकाल के मित्र श्री ललित कुमार मालवीय जी और उनकी धर्मपत्नी को साथ लेकर, मुलाकात का समय पूर्वनिर्धारित किये बिना ही पंडित छन्नू लालमिश्र जी के आवास पर आ धमका । चारों बिनबुलाये, अपरिचित अतिथियों का पंडित जी ने अत्यन्त सहजता एवं आत्मीयता स्वागत किया और स्नेहपूर्वक अपने पारिवारिक “अक्षयपात्र” से सबके लिए बनारसी कचौड़ी और गुलाबजामुन भी प्रस्तुत किया।
कुछ सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर छन् लाल जी ने डाँटते हुए सा कहा “अरे, खाना हो या गाना दोनों ही उचित समय और स्थिति में, श्रद्धापूर्वक, शांतचित्त होने पर शोभा देते हैं – मनमाने समय और तरीके से, जब- तब, जो कुछ भी, मनमर्जी से खाना और गाना उचित नहीं। फिर मैंने “ट्रैक २” डिप्लोमेसी को अपनाया और समसामयिक सांस्कृतिक परिवेश और परिवर्तन, उनकी अपनी प्रेरणास्पद जीवनयात्रा; संगीत की अनेक विधाओं और विविध कथ्य विषयों पर उनकी अदभुद पकड़; तथा तुलसी कबीर की रचनाओं; हिंदी, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा के साहित्य तथा शिव-राम और कृष्ण भक्ति भावनाओं को जनसामान्य के कल्याण के लिए प्रस्तुत करने में अभूतपूर्ण सफलता पर परिचर्चा प्रारम्भ की। इस चर्चा में लगभग डेढ़ घंटे कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला और बिन मांगे ही पंडित छन्नू लालमिश्र जी से उनके कई लोकप्रिय रामचरितमानस के दोहे- चौपाइयों के साथ चैती, कजरी, होरी आदि के टुकड़े भी सस्वर सुनने का सौभाग्य मिल गया। वे मधुर स्वर अभी तक अतःकरण में संचित है।

पंडित छन्नू लालमिश्र जी गायकी की प्रगल्भता के पीछे उनकी दार्शनिकता, उनका लोकसाहित्य का गम्भीर ज्ञान रहा है। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कलाओं में विषेशतः संगीत को शास्त्रीय, अर्द्धशास्त्रीय, ग्राम्य और वनवासी श्रेणियों भाषाओं और बोलियों विविध शैलियों के स्वरूप के आधार पर; खंडित कर उनमें भेद, ऊँच-नीच आरोपित करना अनुचित है और कोरी अज्ञानता और मानसिक – क्षुद्रता का द्योतक है। भारतीय पारम्परिक संस्कृति और सामाजिक चेतना में समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय, सभी प्रकार की सृजनशक्ति – भौतिक संरचनायें और बौद्धिक सर्जना, साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिक चिन्तन मनन की प्रक्रियायें परस्पर निर्भर, जालवत जुड़ी-बुनी हुई हैं। वे सभी अपने अपने प्रभाव से, पूरे समाज को, विभिन स्तरों पर ओत-प्रोत किये हुए हैं। यह ऐक्य परिदृश्य भारत की पारम्परिक लौकिक दैनन्दिन जीवन – यापन में सबसे स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी शासकों द्वारा थोपी गई मैकाले की अंग्रेजी-शिक्षा (जिसमें सफलता ‘लिटरेसी’ संख्या से और ‘डिग्री’ के स्तर से नापी जाती है न की जागतिक अनुभव जन्य ज्ञान और नागरिक चरित्र – निर्माण के मापदंड पर) ने भारतीय समाज इस शताब्दियों से चली आ रही सर्वसमावेशी, सौहार्द्रपूर्ण और साहचर्य की प्रवृत्ति को छिन्नभिन्न कर, अलग-अलग, छोटी-छोटी, परिधियों में घेर रखा है।
गायन भी भारतीय ऋषियों और तत्वदर्शियों के लिए केवल कंठ और मुख तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके चार स्तरों की परिकल्पना की गई है परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इनमें केवल अंतिम स्तर पर, ‘वैखरी’ में ही, ध्वनि ‘मुखरित’ होकर श्रव्य बनती है। शेष, प्रथम तीन स्तिथियाँ आतंरिक हैं, जहाँ न भाषा का भेद होता है और न शास्त्रीय लोक सांगीतिक लक्षणों का; न उत्तरी दक्षिणी गायन पद्धतियों, न ही विविध घरानों की गायन परम्पराओं और अभिव्यक्ति की शैलियों (जैसे ख्याल, कजरी, चैती, ठुमरी आदि) के नाम पर ही विभेद करने की कोई सम्भावना रहती है। परा स्वरुप में तो सब “एकमेवं अद्वितीयं” की वास्तविकता ही विद्यमान होती।

इसी कारण पंडित छन्नू लालमिश्र जी जब अपनी मस्ती में रमकर “स्वान्तःसुखाय” जब भी गाते थे – चाहे अवधी, हिंदी, भोजपुरी, ब्रज या संस्कृत में; चाहे कबीर, तुलसी, रविदास की रचनाओं या लोकगायिकों की पारम्परिक क्षेत्रीय कृतियों को आधार बनाये; चाहे किसी भी रस (श्रृंगार लास्य, हास्य-करुण, रौद्रवीर और वीभत्स आदि) को मूल मानकर आरम्भ करें, धीरे-धीरे अंदर डूबते डूबते सभी अन्ततः एकरस और एकभाव, भक्तिमय हो जाते थे।
यद्यपि जन्म का मृत्यु के साथ अटूट, अपरिहार्य सम्बन्ध है किन्तु सत्य साधकों और भक्तों को शरीर की नश्वरता को लेकर भय नहीं होता क्योंकि उनके परोपकार प्रेरित कृतित्व के यशः काय को जरा मृत्यु की त्रासदी नहीं सताती। जैसे जलबिन्दु अपनी लघुता के कारण क्षणिक अस्तित्व वाला होता हुआ भी जब महासागर में मिलकर विशालता और अमृतत्व प्राप्त करता है उसी प्रकार एक भक्त, साधक भी घट के नाश होने पर घटाकाश के अनन्त आकाश में मिल जाने की तरह देह की सीमा को त्याग कर शिव-सायुज्य में सच्चिदानंद की सातत्य का अनुभव करता है।
सभी भारतीयों विषेशतः बनारस के संगीत प्रेमियों की ओर से, जिनके सबके लिए पंडित छन्नू लालमिश्र जी’ अपने परिवार के सदस्य जैसे ही थे’, उनकी स्मृति शेष और प्रेरणास्पद अक्षयकीर्ति को सादर प्रणाम और हार्दिक श्रद्धांजलि ।
बूंद समाना समुंद में जानत है सब कोई,
समुंद समाना बूंद में बूझे विरला कोई।
डॉक्टर नम्रता मिश्र सुपुत्री पंडित छन्नू लालमिश्र जी
अखिलेश मिश्र (अखिलेश मिश्र) आयरलैंड में भारत के राजदूत